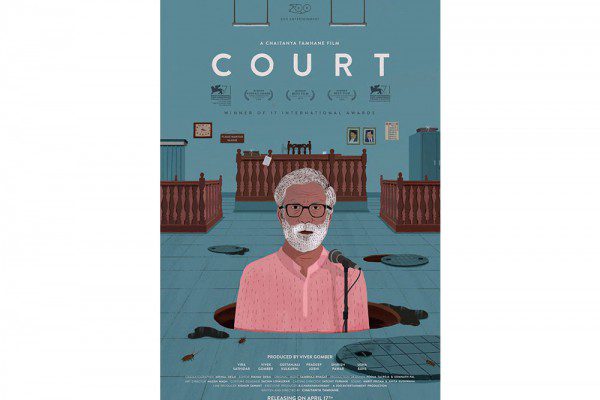ममममाफ़ कीजिएगा, ये मेरा जुमला नहीं, अदबी रवायत के एक बेहतरीन अफ़सानानिगार, जनाब सआदत हसन मंटो साहेब का तकियाक़लाम है. अक्सर चीज़ों को सुनने और देखने के बाद यह जुमला उनकी ज़ुबान पर होता था. बिना इसकी परवाह किए कि किस्सा, कहानी या स्क्रिप्ट सुनाने या लिखने वाले के दिल पर इससे क्या गुज़रेगी, वो अक्सर इस जुमले से बाकी तमाम लोगों को नाप देते थे. ऐसा कतई नहीं था कि मंटो किसी तय तुनकमिजाज़ी की वजह से या किसी ग़लतफ़हमी के शिकार होने के चलते ऐसा करते थे, चुनाचे उनकी ज़बान पर यह जुमला इसलिए आ जाता था क्योंकि मंटो दुनिया को बहुत सहज और सीधा-सीधा देखना पसंद करते थे, बाकी लोगों की तरह ओढ़-बिछा, ढक-छिपा के नहीं. मंटो की इसी तबीयत के सामने जब ऐसी बातें या तहरीरें पेश आती थीं, जिनमें ऐसे ही किसी बनावटीपन की बू होती या उन्हें मालूम देता कि कोई अल्फ़ नंगा और खोखला होते हुए भी सूट-शेरवानी में समाया जाता है तो अक्सर बोल पड़ते थे…. फ़्रॉड है यार… सब फ़्रॉड है.
न, आप ऐसा कतई मत समझिए कि मेरी आज तबीयत मंटो पर कुछ लिख मारने की और फिर अपने कानों में मंटो के इसी जुमले को गूंजता हुआ महसूस करने की है. अव्वल, मेरा इस तरह मंटो के जुमले को आपके पेशे नज़र ले आने के पीछे का इरादा दरअसल कुछ और है. तो जनाब हुआ यों कि दिल्ली में पिछले दिनों अपने दो फ़नकार दोस्तों को, जिनको ज़्यादातर लोग उनकी दास्तानगोई की हुनरमंदी की वजह से जानते हैं, मैंने मंटो के बारे में एक दास्तानगोई का प्रोग्राम पेश करते हुए सुना… ऐसे तमाम लोगों के साथ, जो अदबी इदारों के माहिल और माहिरीन हैं या शहरी ज़िंदगियों में एक ख़ास किस्म के तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनके बीच ऐसी तमाम खुशतबीयत करती चीज़ों के शौक फ़रमा होते हैं. वैसे, दास्तानगो जनाब महमूद फ़ारूक़ी और दानिश हुसैन दिल्ली क्या, कई शहरों में और बाहर भी पहचान के सिलसिले में एक ख़ास मकाम रखते हैं और उनका आपसे तार्रुफ़ कराने के लिए अलग से किसी वरक की ज़रूरत नहीं है. पर फिर भी, ऐसे तमाम लोगों के लिए, जो दास्तानगोई की रवायत या इन दोनों लोगों से वास्ता नहीं रखते या इन्हें नहीं जानते, उनके लिए मैं बता दूं कि दास्तानगोई अय्यारों और तिलिस्मों की कहानी को ख़ास किस्म से पेश करने की एक रवायत है जिसके ज़रिए लोग एक ज़माने में शामों, महफ़िलों में अपना मनोरंजन करते थे. यह परंपरा अब खत्म सी है. कुछ है जो इन दो हुनरमंदों ने संभाल रखा है, बाकी पुरानी रवायत के घर और पेशेवर परिवार अब लगभग खत्म हो चुके हैं क्योंकि इनकी परवाह न सरकारों को रही, न रहनुमाओं को और न ही बदलते दौर में कहानियों और किस्सों को सुनने वाले रहे. बल्कि यूं कहें कि ज़िंदगी इस क़दर तकनीक के डिब्बों में क़ैद होती गईं कि दास्तानगोई खानबदोश मौत मर गई.
बहरहाल, तो जैसा कि होता है, दास्तानगोई में एक बात कहो तो उससे और कई बातों का सिलसिला सा निकल आता है. यही फिलहाल मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, जब आप इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं और मुझे तमाम गालियों से नवाज़ते जा रहे हैं कि ये भी क्या ख़ूब बेवकूफ़ और आला दर्जे का बेहूदा इन्सान है कि जेहन में किसी बात को सुनने की एक खुजली सी पैदा करके कभी मंटो तो कभी दास्तानगोई के मसले और मायने झौंके जा रहा है. जनाब, ग़ुस्ताख़ी माफ़. मैं असल मसले पर आता हूं.
असल मसला है मंटो का जुमला- फ़्रॉड है यार… सब फ़्रॉड है. महमूद और दानिश बार-बार इसे दोहरा रहे थे और जैसे-जैसे वो इसे दोहराते जा रहे थे, मैं पुरतबीयत दिल्ली के आलिशान इंडिया हैबिटेट सेंटर के उस हॉल में बैठे लोगों को देख रहा था और इस जुमले पर और ज़्यादा यकीन करता जा रहा था. अव्वल तो कुछ देर बाद यूं मालूम देने लगा कि लखनवी अचकनों में सजे-लिपटे दास्तानगो न हों, बल्कि खुद मंटो मंच पर मौजूद हों… एक लंबे कॉलर की कमीज़ पहले, जिसके दो बटन खुले हैं. बाल बिखरे हैं, पास में सिरगेट की एक डिब्बी और माचिस है. कुछ कागज़ और ख़त बेतरतीब बिखरे हैं. दुमड़ी हुई चादर और तेल में चिकनी हो चली मसनद पर टिके मंटो ने नीचे एक पतलून या पजामा पहन रखा है. आंखों पर एक अदद ऐनक है और शीशे कितने भी धुंधले हों, पूरा चीरकर देखने वाली नज़रें उनके पीछे मौजूद हैं और उस हॉल में बैठे तमाम अवाम को देखकर मंटो खुद बार-बार सिगरेट का टोटा किसी कटोरी या दिये में रगड़ते हुए कह रहे हैं- फ़्रॉड हैं यार… सब फ़्रॉड हैं.
दास्तानगोई के इस प्रोग्राम में शिरक़त के लिए एक तय टिकट था. यह टिकट अपनी जेब की हद से बाहर था इसलिए अपन ने यह तय पाया था कि यह दास्तानगोई किसी बड़े आदमी के बेडरूम की चादर के माफ़िक है जिसे न तो देखने की किस्मत है और न उसपर सोने की. पर शाम होने को आई ही थी कि एक नामचीन और ख़ास इदारे की हमारी एक जाननेवाली साहिबा का फोन आया, अपने पास छह लोगों के लिए पास हैं… क्या चलना पसंद करोगे. मैंने न्योते के इंतज़ार में बैठे भूखे की तरह फ़ौरन हामी भर दी. तय वक़्त पर पहुंच भी गया. बाहर दानिश मिले और महमूद भी और उसके बाद जिधर नज़र कीजिए, बस एक से बढ़कर एक अव्वल लोग. नामचीन, बड़े अहोदे वाले और वालियां, फ़ैब इंडिया की साड़ियां, यूसीबी की टीशर्टें, बेहद महीन कमीज़ें, ख़ास किस्म के इत्र में नहाए, नक्शो-निगार पर न तो मौसम का कोई असर था और न उम्र का. उजले गुलाबों की तरह- खिले-खिले और कीमती मालूम देते. मैं सोचने लगा कि मंटो इस महफ़िल में शामिल होने की कोशिश करते तो दरबान ही हांककर बाहर कर देता. कहता- कहां घुसे जा रहे हो. इस थैले में क्या है और इतनी शराब पी रखी है. यह कोई मज़ार है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए. सकुचाते हुए मैं भी कतार में लगा-लगा इन शरीफ़ों के साथ हॉल में दाखिल हुआ. अंदर देखा तो हर उम्र के लोग कुर्सियों पर तशरीफ़ पा चुके थे. कुछ बाज मुल्कों के अंग्रेज़ लोग भी थे. बाकी के हिंदोस्तानी थे जिनमें से अधिकतर का दास्तानगोई की ज़ुबान, हर्फ़ों, हुनर, रवायत, अंदाज़ जैसी चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था. हाँ, एक बात बहुत अच्छी थी कि हर उम्र के शरीफ़ यहाँ मौजूद थे. मसलन, स्कूल जाने वाले जवान होते बच्चे, उनकी मांए और दादियां, दादा और नाना, कुछ बेवाएं, कुछ अकेले ज़िंदगी काट रहे अधेड़. इन सबमें एक बात ही सबको एक ही डोर से बांधती दिखती थी और वो थी उनका एक ही क्लास से होना. अव्वल यूं जान पड़ता था कि बड़े घरों के लोग दुनिया के इतने बदल जाने के बाद भी मनोरंजन और उसके बाद कुछ खाने-पीने के लिए शाम होते घरों से निकलते हैं. आज एक ख़ास किस्म के तमाशे से रूबरू होने का मौका है. ममा, वॉट इज़ दास्तानगोई… इट्स नॉट इज़ी फ़ॉर मी टू अंडरस्टैंड. लुक एट देअर ड्रेस… मस्ट बी डिज़ाइनर वियर. वाए दे हैव टू कैंडल्स… वाओ, दे ड्रिंकिंग समथिंग इन सिल्वर बओल्स. बगल की सीट से कोई जनाब यूं पलटकर देखते जैसे सब समझ रहे हों और ये सवाल उनके मनोरंजन में ख़लल पैदा कर रहे हों और फिर ये नई उम्र के बच्चे एक मजबूर शराफ़त के हाथों मारे जाते, बेचारे अपने ब्लैकबेरी पर कुछ लिखना-पढ़ना शुरू कर देते.
मंटो की ज़िंदगी का सफ़र मंच से सुनाई देता रहा. पर अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद ही मंटो को पढ़ा हो. जिन्होंने पढ़ा भी था, उनको मंटो की कहानियों के अंग्रेज़ी तर्जुमे किसी बुकस्टोर से मिले थे. जैसे कि- सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ मंटो, मंटो-दि ग्रेट उर्दू राइटर, वगैरह-वगैरह. अक्सर ऐसा पाया जाता है कि दुनिया के तमाम अंग्रेज़ी या फ्रांसिसी, जर्मन और स्पैनिश लेखकों, कवियों को पढ़ते हुए और फिर भारतीय या भारतीय मूल के अंग्रेज़ी अदीबों की गलियों से गुज़रते हुए इस क्लास के लोगों को अगर ग़ालिब, कबीर, प्रेमचंद और मंटो के अंग्रेज़ी अनुवाद मिल जाएं तो वे फ़र्ज़ अदायगी के लिए इनको भी पढ़ लेते हैं. मैंने अक्सर दिल्ली की ऐसी महफ़िलों में पाया है कि इस क्लास के हज़रात-ओ-खवातीन अपने भाषणों में अंग्रेज़ी के ही लेखकों को या कवियों को कोट कर रहे होते हैं. मज़ाल है जो कभी निराला, तिरुवल्लुवर, धूमिल, नज़ीर, मजाज़, फ़ैज़, हबीब जालिब, सर्वेश्वर दयाल, अदम जैसों का ज़िक्र भी आ जाए. क्या पता नाम तक न मालूम हो.
मुझे दास्तानगोई में मज़ा भी आ रहा था और मौजूद लोगों पर, इस प्रोग्राम पर हंसी भी आ रही थी. मालूम देता था कि या तो किसी अंग्रेज़ को पान खिलाने की कोशिश की जा रही है और या फिर किसी पूर्वांचलिए भतखोर भाई को फ़िश एंड चिप्स का डिनर कराया जा रहा है. एकदम उलट जुगलबंदी. मंटो होते तो पैर पटकते हुए बाहर चले जाते… दो मिनट से ज़्यादा ऐसा होता बर्दाश्त न करते. ग़नीमत है कि नहीं थे. ख़ैर, मेरे मसले से शायद आप वाकिफ़ हो गए हों. यह भी मुमकिन है कि मुझे फिर से गालियां दे रहे हों कि बताइए भला, क्या इस क्लास के लोगों को दास्तानगोई सुनने का कोई हक़ ही नहीं है. बिल्कुल है जनाब पर बंदरों को दाल चावल खिलाने से पहले भूखे इंसानों के बारे में भी सोचिए. मदरसों, स्कूलों, बस्तियों, गांवों में वो लोग और वो ज़ुबान बसती है जिसमें मंटो अपनी बात कहते थे. उनके पात्र भी अक्सर उन्हीं के बीच के थे. पर ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसी तमाम जगहों पर न तो ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं और न ही उनतक मंटो को पहुंचाने की कोई ईमानदार कोशिश की जाती है.
राजाओं की महफिल वाला स्वांग कबतक चलेगा. कोट पैंट पहनने वाले जागीरदार कबतक संस्कृति और कला को अपनी रखैल बनाए रखेंगे और उनतक पहुंचने के बाकी लोगों के रास्ते कबतक बंद रहेंगे. क्यों ऐसा होता है कि ऐसे शो के अधिकतर टिकट उन घरों के लोगों को मुफ़्त मिल जाते हैं जो रोज़ लाखों कमाते हैं और ऐसे लोग तरसते रह जाते हैं जिन्हें इस कला से प्यार है पर जेब में टका तक नहीं है. मंटो, प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध भूख के पेट में रोटियों के लिए तरसते चल बसे और उनके किस्सों का मज़ा भरे पेट के ऐसे जाहिलों को नसीब हो रहा है जो समाज में सबसे ज़्यादा शरीफ़, अक्लमंद, तरक्कीपसंद और आधुनिक होने का दावा पेश करते हैं. मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर. शर्म और दया आती है ऐसी शक्लों पर जिनके लिए कला और संस्कृति अजायबघर के नमूनों की तरह हैं, संग्रहालयों की मूर्तियों की तरह हैं. ऐसे ही लोग कमानी ऑडिटोरियम की कुर्सियों में घंसे मिल जाते हैं. ऐसे ही लोग इंटरनेशनल सेंटर के सभागारों में, ऐसे ही लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुतियों में. हर तरफ़ इनका कब्ज़ा. इन्हीं के लिए टिकट, इन्हीं के लिए पास, इन्हीं के लिए इंतज़ाम, इन्हीं के लिए शाम, इन्हीं के लिए प्रस्तुति, इन्हीं के लिए स्तुति… सबकुछ इन्हीं का. पानी की बोतल भी, पिज़्ज़ा का कोना भी, बियर का कैन भी, एयरकंडीशनर कारें और साउंडप्रूफ़ सभागार भी, सजावटें और संस्कृतिकर्मी भी. बाकी स्याले मरें मंटो की मौत.

मैं बैठा-बैठा बड़बड़ाने लगा. जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो लिहाज छोड़ अपने झोले में हाथ डाला और पान का बीड़ा निकाल किया. उंगली पर चूना जमाया, एक दांत से ज़रा सा काट कर पान के साथ चुभलाया. थोड़ी सी तंबाकू दबाई और मंटो के बारे में सोचते-सोचते कभी मुंबई, कभी आगरा, कभी पाकिस्तान और कभी वापिस दिल्ली तक आता-जाता रहा. तालियों की आवाज़ से ध्यान टूटा. इल्म हुआ कि महफ़िल इख़्तताम पर पहुंची. चुनाचे यह पता नहीं कि लोग किसी अंजाम पर पहुंचे या नहीं.
मंटो होते तो इस महफ़िल को एक ही लाइन में नाप देते- फ़्रॉड हैं सब… सब फ़्रॉड हैं.