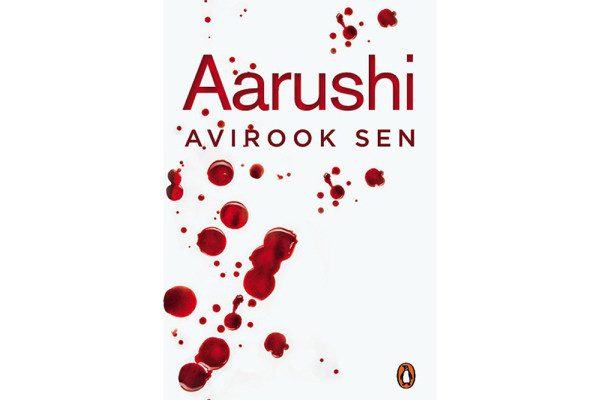पिछले दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किंडल पत्रिका की ओर से आयोजित एक संगोष्ठी में जाने का मौका मिला. विषय था- डायलेक्टिक्स ऑफ़ लॉस. संवाद के लिए कलाकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले सारनाथ दा हमारे बीच थे. हानियों, नुकसानों के इस तर्कशास्त्र की चर्चा करते हुए हमने लंदन ओलंपिक के दौरान के उनके कुछ रेखाचित्रों, कलाकृतियों को भी देखा. दरअसल, वे चाहते थे कि ओलंपिक खेलों के दौरान इन खेलों के दूसरे पहलुओं की चर्चा करते हुए हानियों या नुकसानों, तकलीफों की पारिस्थितिकी को समझा जाए. इसीलिए उनकी चर्चा की धुरी इन रेखाचित्रों के इर्द-गिर्द घूम रही थी. मैं बहुत कौतुहल के साथ इन चित्रों को देखता चल रहा था. समझने की कोशिश कर रहा था कि क्षतियों के दर्शन और उनके व्यवहारिक जगत के बीच कलाकार कहां गोते लगा रहा है और क्या स्थापित करना चाह रहा है.
सारनाथ के तर्क रोचक थे. इन चित्रों में उन लोगों को चर्चा थी जो खेल नहीं सके. जो खेले पर हारे. जो हारते रहे पर कोशिश करते रहे. जो हारे हुए लोगों के बीच से आते हैं. ऐसे भी, जो खेल नहीं सकते पर खेल रहे हैं. इन सारे लोगों के बीच हार (इसे व्यापक करके देखूं तो नुकसान, क्षति, तकलीफ़ जैसे कई मिश्रित शब्द कौंध जाते हैं) का तर्कशास्त्र मुख्यधारा के साथ टकराता नज़र आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि जीत का बाज़ार सिक्के पर छपी अशोक की लाट की तरह है और सारनाथ सिक्के को थोड़ा सा उठाकर उसके नीचे दबे दूसरे पहलु पर अपने दर्शन और तर्क को केंद्रित करना चाहते हैं.
उनकी बातों के और संवाद के दौरान अब मैं हानियों के एक विस्तृत संसार में जा चुका था जहां सारनाथ बहुत पीछे छूट गए लगते थे. निःसंदेह, वो मेरे प्रति नहीं, अपनी सोच और रचनात्मकता के प्रति उत्तरदायी हैं. पर दर्शक या श्रोता के पास जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है मुल्यांकन और इससे न तो सारनाथ मुझे रोक सकते थे और न ही कोई और.
उनका दायरा उनकी बौद्धिकता, विमर्श और रचनात्मकता थी. ओलंपिक इस विषय का उदाहरण था पर अब मैं उस हॉल में बैठा कौड़ियों के खेल याद कर रहा था. ज़मीन पर चौखटा काटकर पतली गिट्टक को ठोकर मारकर पाले लांघने के खेल याद आ रहे थे. याद आ रहा था पांच गिट्टियों से टाइमिंग और बैलेंस को समझाने वाला खेल, जो अक्सर अपनी दोनों टांगे पसारकर लड़कियां खेलती दिख जाती थीं, कभी कुंए की जगत के पास, कभी नीम के चौतरे तले, कभी मंदिर के दालान में, घर के आंगन में तो कभी गर्मियों की शाम घरों की छत पर. कंचे, गुल्ली-डंडा, नदी-पहाड़, खट-खट, चौपड़, आइस-पाइस, विष-अमृत… हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कित्ता पानी- कानों में गूंज रहा था. पोशंपा भई पोशंपा, डीप-डीप-डीप, बचपन की रसोई के बहाने पिसान की चिड़ियों के खेल और मिट्टी की बर्तन बनाने की कोशिशों में टैराकोटा का अपना बेसिक अध्याय. धनुष-तीर, खेतों में बिजूका को देखकर उसकी जैसी भंगिमाएं बनाने और मेड़ के किनारे बैठ उसपर मिट्टी की गाड़ी दौड़ाने के खेल. साइकिल के टायरों को लकड़ी के एक हत्थे से हांकते या मोटरसाइकिल की बैरिंग को एक छड़ी में जड़ी कील के सहारे कस्बे भर में सड़कों, पगडंडियों और नहर किनारे दौड़ाते हुए सैकड़ों मीटर दौड़ना. हम उस बचपन में बड़े हुए जब बैट-बल्ले से पहले एरेंड के बीज, इमली के बीच, जंगलजलेबी के दाने, कौड़ियां, आम की गुठलियां और सरकंडे के फूल हमारे खेल के साधन होते थे.
मैं फिर लौटा अपनी इस विचार यात्रा से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उस हॉल में जहाँ सारनाथ दा ओलंपिक के दूसरे अनकहे पहलुओं के ज़रिए हानियों की अंतर्कथा समझा रहे थे. पर इस कथा में मेरे ये खेल तो थे नहीं. तो क्या हानियों का, नुकसानों का और दूसरे पहलुओं का संसार भी वहीं उसी बाज़ार के सापेक्ष खड़ा रखा जाएगा जहाँ एक सजा-धजा और वैश्विक मान्यता वाला खेलतंत्र खड़ा है. क्या हम बीरबल हैं जो दरबार में खींची गई लकीर के बराबर में अपनी एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. तो फिर उनका क्या, जिन्हें बाज़ार ने मान्यता नहीं दी. जो दरबार में न कभी आए और न ही दरबार ने उन्हें कभी मान्यता दी. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हानियों के एक क्लास करेक्टर में उलझ गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे. विरोध करते हुए भी उसी नांव पर सवार हैं जो बाज़ार की लहरों पर तैर रही है.
हानियों का विस्तार इससे कहीं आगे तक पसरा नज़र आता है. जो खेलकर हारते हैं, उनकी पराजय को क्या उनके साथ जोड़कर देखा जा सकता है जिन्हें खेलने ही नहीं दिया गया. जिनको खेलना तो दूर, समाज में उठने-बैठने, पढ़ने, कहने, गाने-पूजने, कहने-सुनने से वंचित रखा गया. जिनकी ज़बानों को सिल के पत्थरों से इसलिए कूंच कर मसल दिया गया क्योंकि या तो वे दलित थे, आदिवासी थे, महिलाएं थीं, गरीब थे, भूमिहीन थे, अल्पसंख्यक थे, व्यवहारिक और प्रगतिशील थे, वर्जनाओं से अलग थे, ग़लत के ख़िलाफ़ खड़े थे. उनका क्या. उन खेलों का क्या- जिन्हें न तो खेल संघों ने पहचाना, न ओलंपिक इकाइयों ने. न सरकारों ने, न समाज और संस्कृति के ठेकेदारों ने. बावजूद इसके कि वे युद्ध के बाद मरे हुए योद्धाओं के सिरों को पैरों की ठोकरें मारकर मज़ा लेने की अमानवीयता से पैदा हुई फुटबॉल की परंपरा के ठीक उलट प्राकृतिक रूप से जन्मे, पनपे और ढले हुए थे.
पराजित सदा से जीतने वालों के इतिहास का हिस्सा रहे हैं. जब पराजितों का ज़िक्र नहीं होगा तो जीतने वाले का इतिहास कैसे स्थापित होगा. इसीलिए राम के साथ चिपके हैं रावण, कृष्ण के साथ चिपके हैं कंस, पांडवों के साथ कौरव, सिकंदर के साथ पुरू, अंग्रेज़ों के साथ गांधी, इंदिरा के साथ जयप्रकाश- ऐसी कई जोड़ियां हैं. पर परित्यक्तों का क्या. किसे मालूम है कि लक्ष्मीबाई की साड़ी किन हाथों ने ताने-बाने पर तैयार की थी. कौन जानता है कि नमक सत्याग्रह में सबसे पीछे चलने वाला कौन था. किसको पता है कि पर्वों पर चौक पूरने- अल्पना बनाने वाली और दीवारों को गेरू से सजाने वाली औरतों के हाथ पर क्या नाम गोदा हुआ था. प्रेमचंद के ईदगाह में जो खिलौने बेचने वाला था, उसके घर कितने दिए जलते थे. सामाजिक क्रांति और भारत की आज़ादी की लड़ाई के अधिकतर योद्धाओं के घर का मैला कौन साफ करने आता था. ताज़महल के कारीगरों को छोड़िए, इंडिया गेट तक के कारीगरों की बस्तियां कहाँ थीं, किसी को मालूम है क्या. विक्टोरिया मेमोरियल के सामने तांगा हांकते-हांकते टीबी से मरनेवालों के नाम किस किताब में दर्ज हैं… परित्यक्तों का बहुमत है पर वो सोचे-समझे ढंग से पूरे डिस्कोर्स से बाहर हैं. आखिर क्यों. क्या ये लॉस के दायरे में नहीं आते. क्या इनकी हारों का हिसाब नहीं होना चाहिए और गुनहगारों को सामने नहीं खड़ा करना चाहिए. कितने कमाल की बात है न कि हम जिसे गाली देते हैं या जिसकी आलोचना करने के लिए खड़े होते हैं, वही हमारी इस पूरी कोशिश के दायरे और भाषा को तय करता है. कितनी चतुराई से हम मकड़ी के जाले में उलझते जाते हैं जहाँ एक तिलिस्म हमें खुद में जकड़े रहता है और हमें लगता है कि हम लड़ रहे हैं, अकड़े हुए हैं, अपनी धार को, तलवार को पकड़े हुए हैं.
मिट्टी के बर्तन बनाता हुआ मैं, जो एक छोटा-सा बच्चा था, अपने अंदर एक कलाकार से मिलता था. शोर को सुर देने की कोशिश करता मैं एक गायक था. पहिए के साथ पगडंडियों पर दौड़ता मैं खुद को पहिए का आविष्कारक समझता था. मुट्ठी में चार गिट्टियां दबाकर पांचवी को हथेली के दूसरी ओर साधते हुए मुझे लगता था कि यह सध गया तो सिर पर धरती साध सकता हूं. पर हानियों के संसार में मेरे ये सारे खिलाड़ी कहीं नहीं मिले उस दिन. न मेरे खेल, न मेरे खिलाड़ी. हम दोनों ही बहुत तेज़ी से खत्म हो रहे हैं. मेरे खेल भी और खिलाड़ी भी.
सारनाथ दा, हम अगली बार आंगन के कुछ खेल खेलेंगे. क्या कहते हैं…?